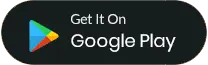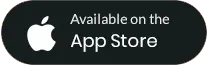केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग को अधिसूचित किया,3 वर्ष का कार्यकाल
 Committee and Commission
6 min read
Committee and Commission
6 min read
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आशय की एक अधिसूचना केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 2 सितंबर 2024 को जारी की गई । भारत के पिछले 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था।
विधि आयोग केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय
विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में विधि आयोग का कोई उल्लेख नहीं है और न ही संसद ने विधि आयोग की स्थापना के लिए कोई कानून पारित नहीं किया है।
विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। इस प्रकार इसकी सभी सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं।
केंद्र सरकार विधि आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि विधि आयोग की रिपोर्टों पर देश में व्यापक रूप से बहस होती है क्योंकि वे उन सदस्यों द्वारा तैयार की जाती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हैं।
भारत के 23वें विधि आयोग की संरचना
भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत के 23वें विधि आयोग में पांच पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीश होंगे।
23वें विधि आयोग में शामिल होंगे:
- अध्यक्ष,
- चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
- पदेन सदस्य के रूप में ,सचिव, कानूनी कार्य विभाग;
- पदेन सदस्य के रूप में, सचिव, विधायी विभाग; और
- अधिकतम पाँच अंशकालिक सदस्य।
23वें विधि आयोग का कार्यकाल
23वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन साल का होगा -1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक।
23वें विधि आयोग के कार्य
विधि आयोग देश की कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव का सुझाव देता है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और इसे अधिक न्यायोन्मुख बनाया जा सके।
भारत सरकार ने विधि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें भी निर्दिष्ट कीं है । 23वें विधि आयोग के कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं
- उन कानूनों की पहचान कारण जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं है।
- भाषा और प्रक्रियाओं को सरल बनाने सहित समय-समय पर समीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करना ।
- उन कानूनों की पहचान करना जिनमें वर्तमान आर्थिक जरूरतों के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है।
- जिन कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है उनमें संशोधन का सुझाव देना।
- नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उपाय प्रस्तावित करना ।
- गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और अधिनियमन के बाद सामाजिक-आर्थिक कानून का ऑडिट करना ।
- मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना।
- अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना और विभिन्न उच्च न्यायालय के नियमों में एकरूपता लाने के लिए सुझाव देना।
- मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना।
विधि आयोग के बारे में
1833 के चार्टर अधिनियम में काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
ब्रिटिश काल में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी।
ब्रिटिश काल में 1834,1853, 1861 और 1879 में चार विधि आयोग स्थापित किये गये।
आज़ादी के बाद
स्वतंत्रता के बाद 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहला विधि आयोग स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड थे। प्रथम विधि आयोग की अवधि तीन वर्ष (1955-1958) की थी।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी (2020-24) थे।